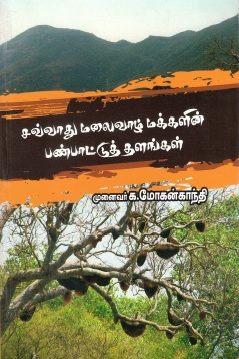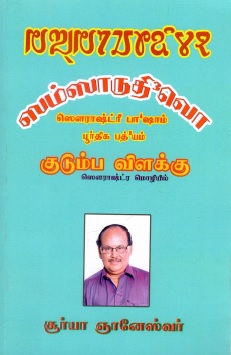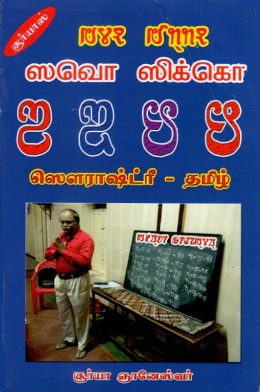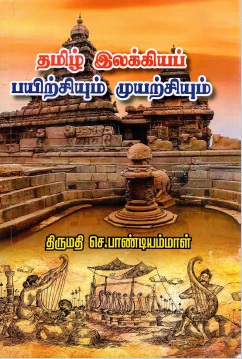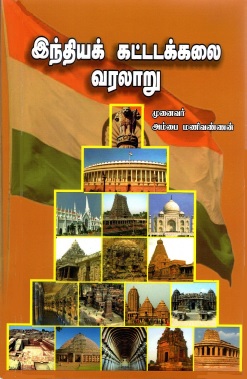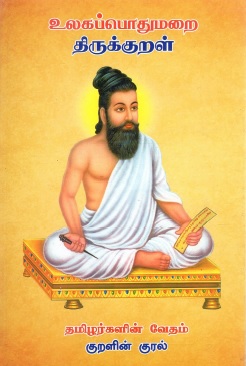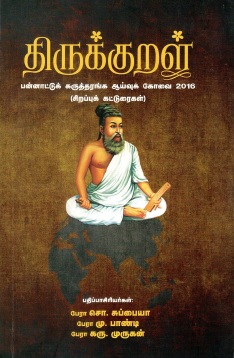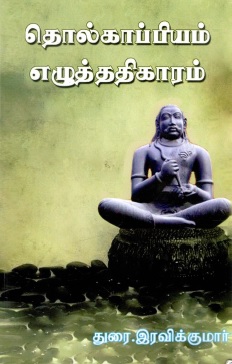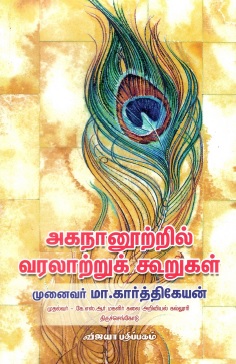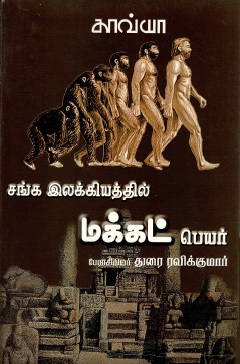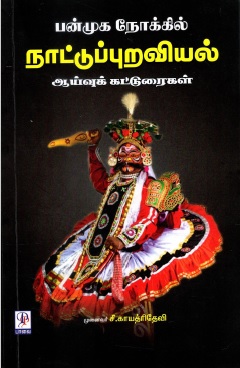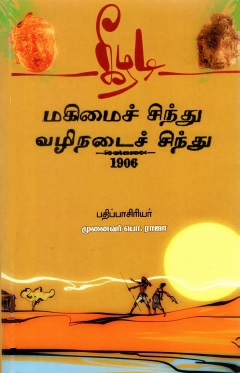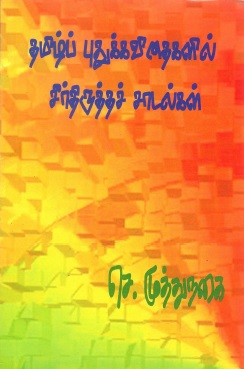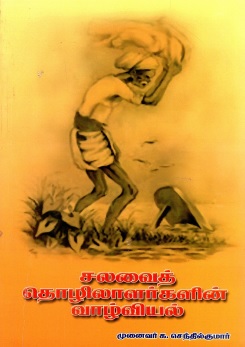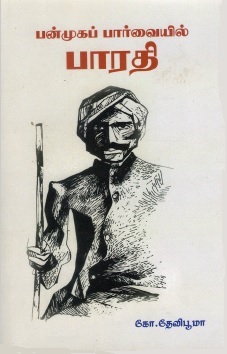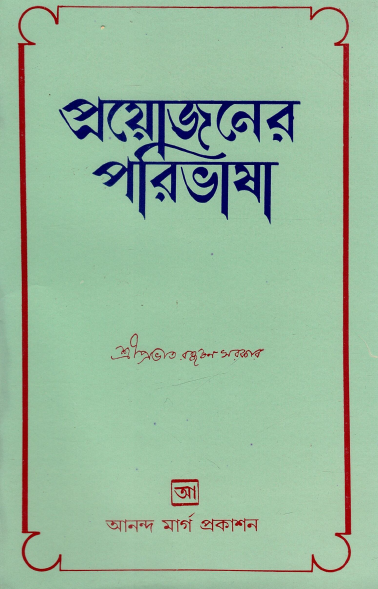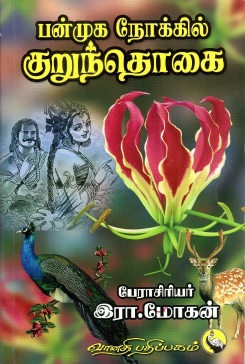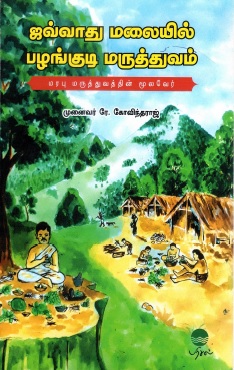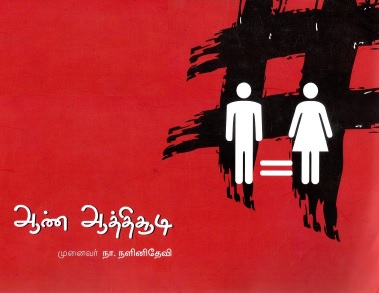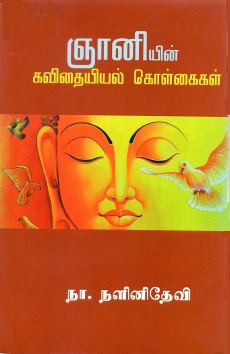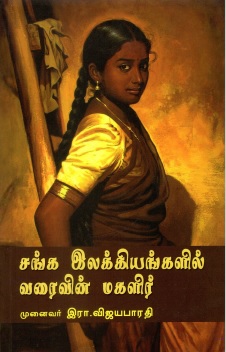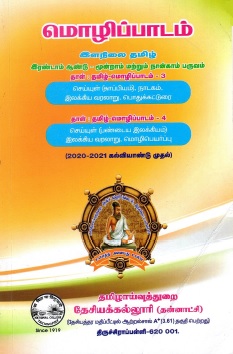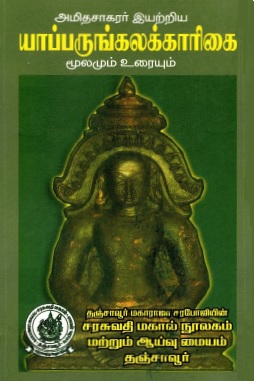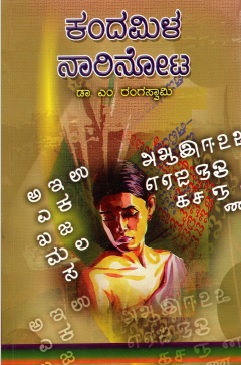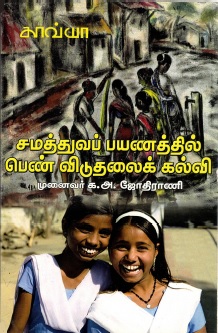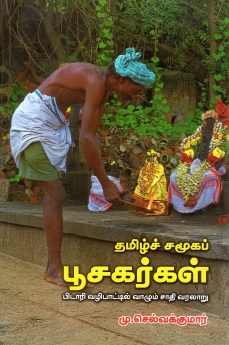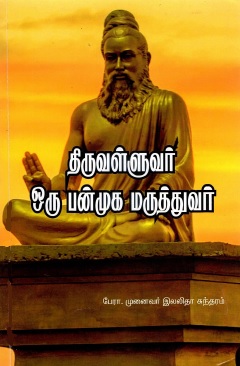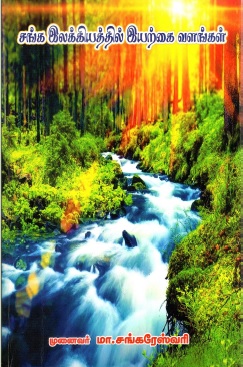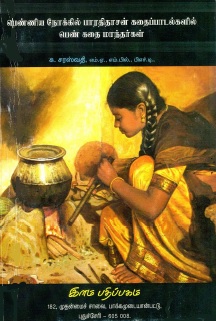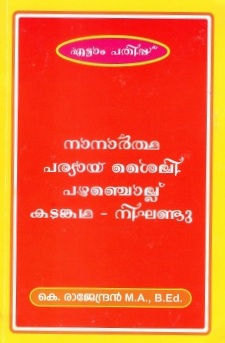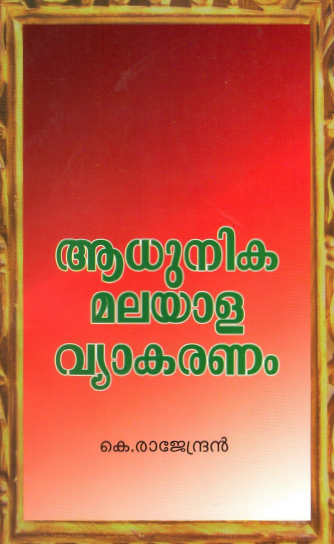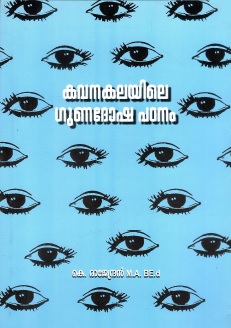Languages
भारतवाणी
bharatavani
bharatavani

Knowledge through Indian Languages












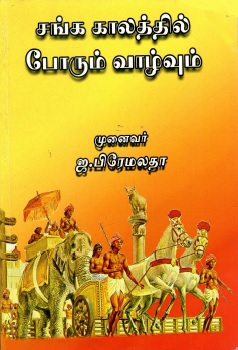

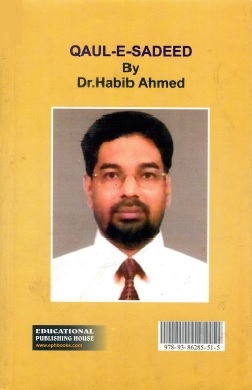
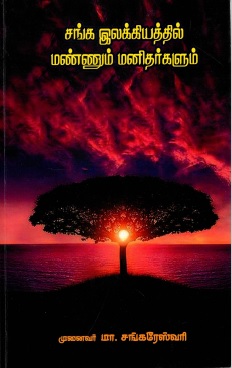
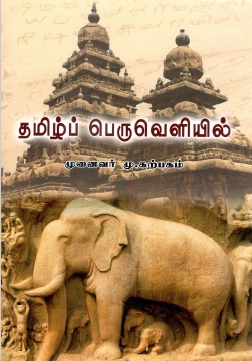
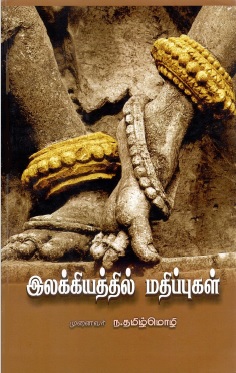
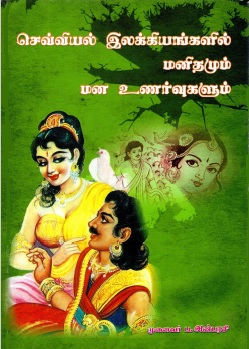
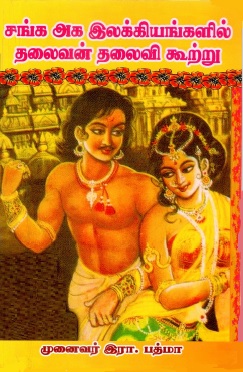
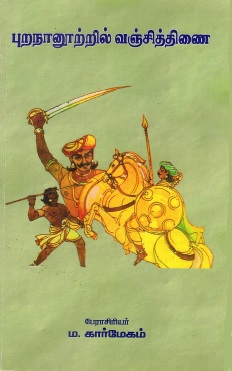
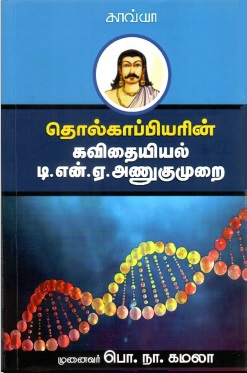
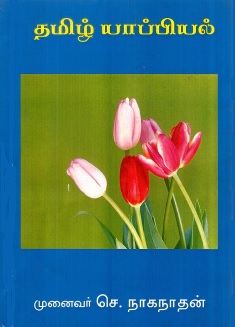
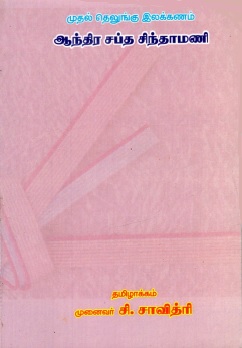
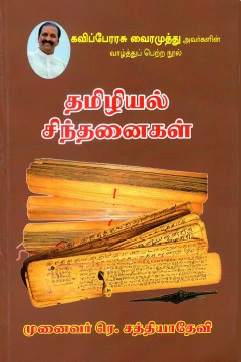
.jpg)
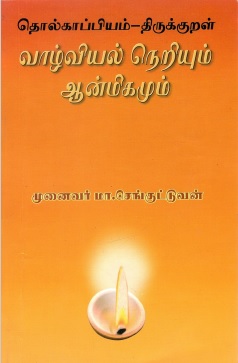
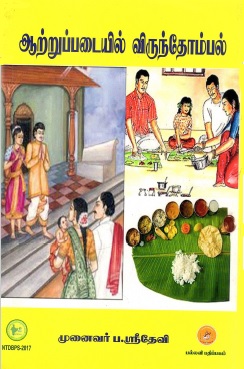
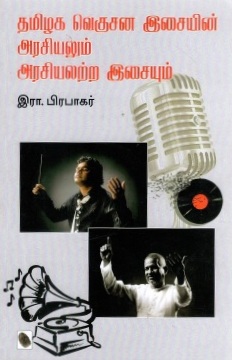
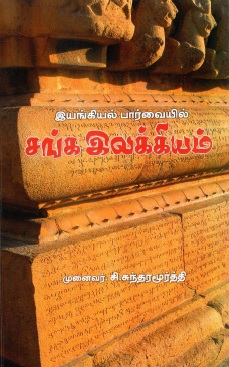
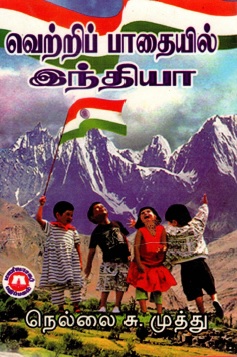
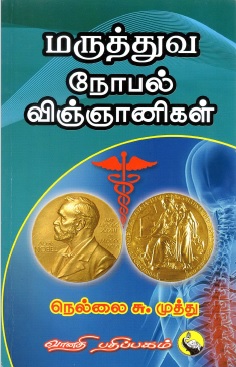
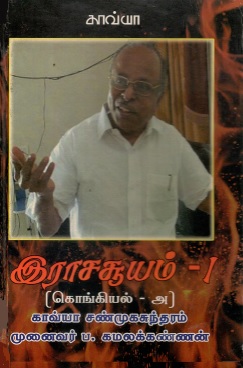
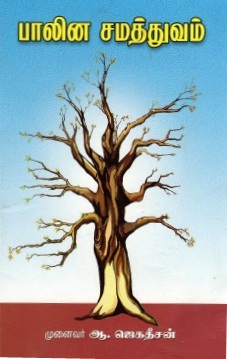
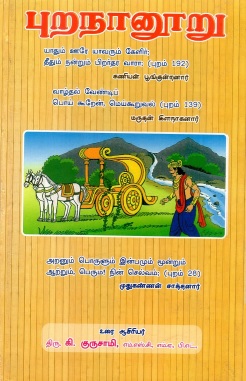
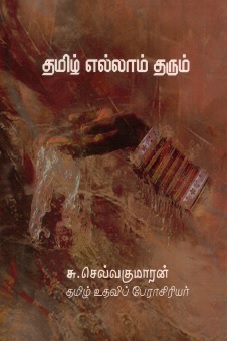
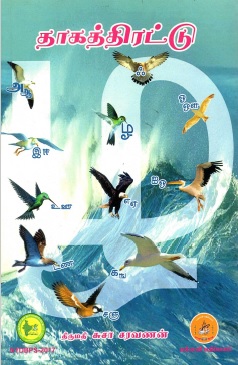
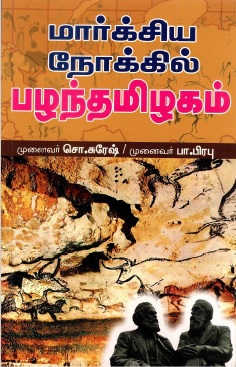
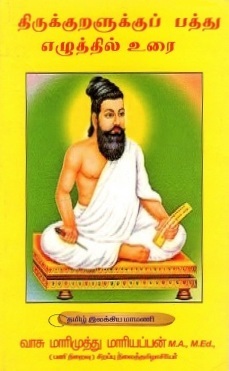
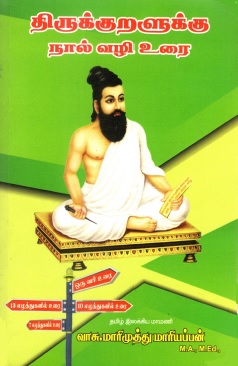
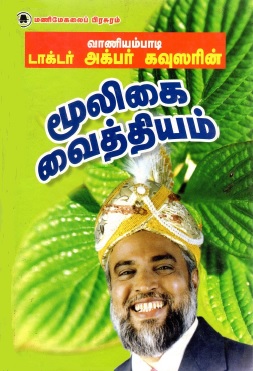
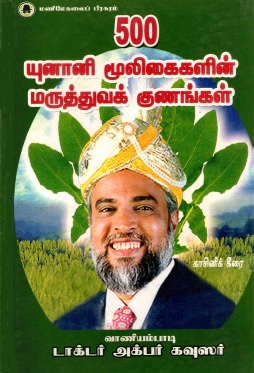
.jpg)