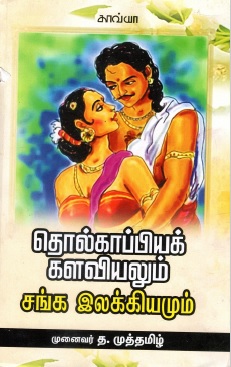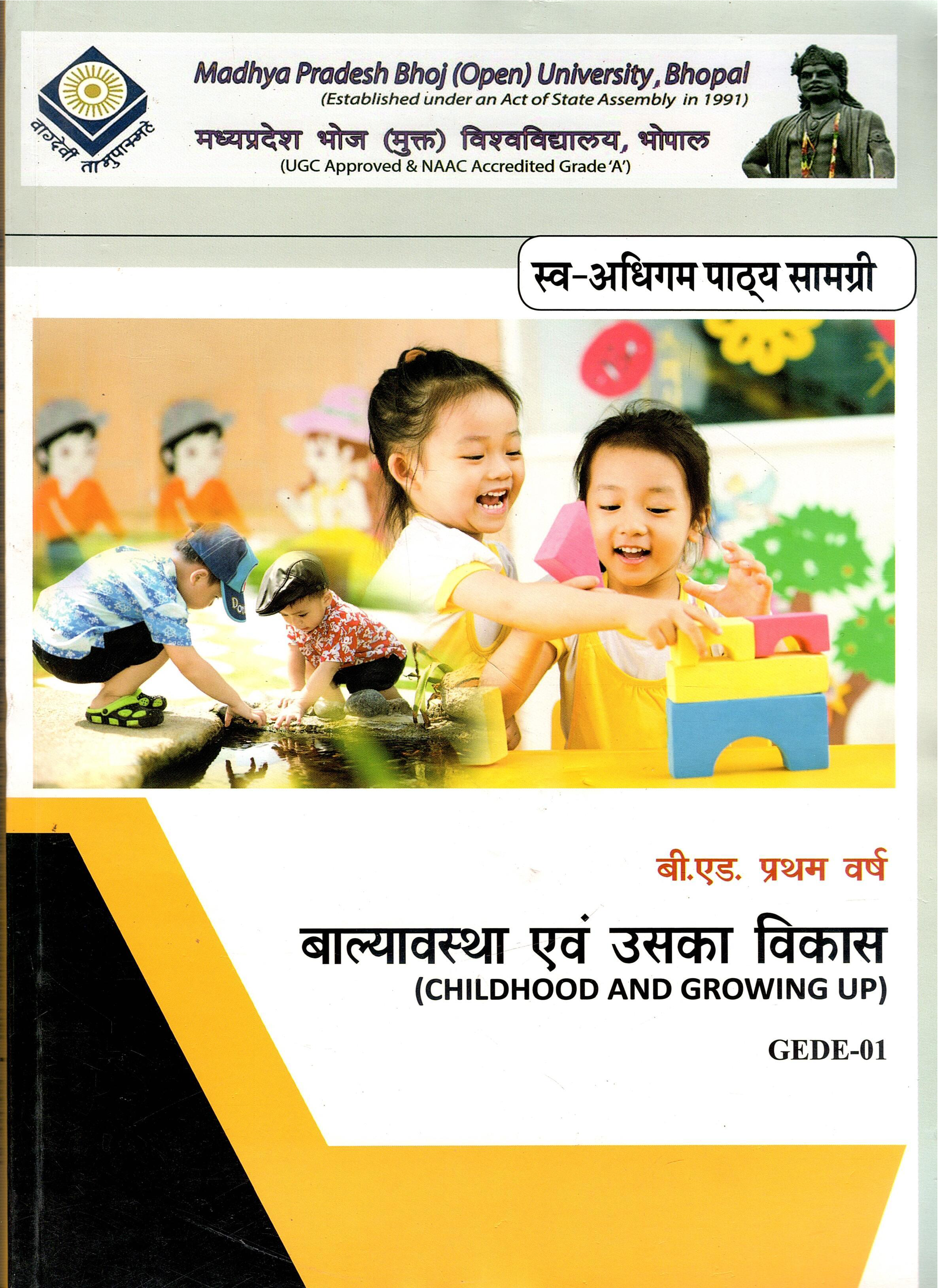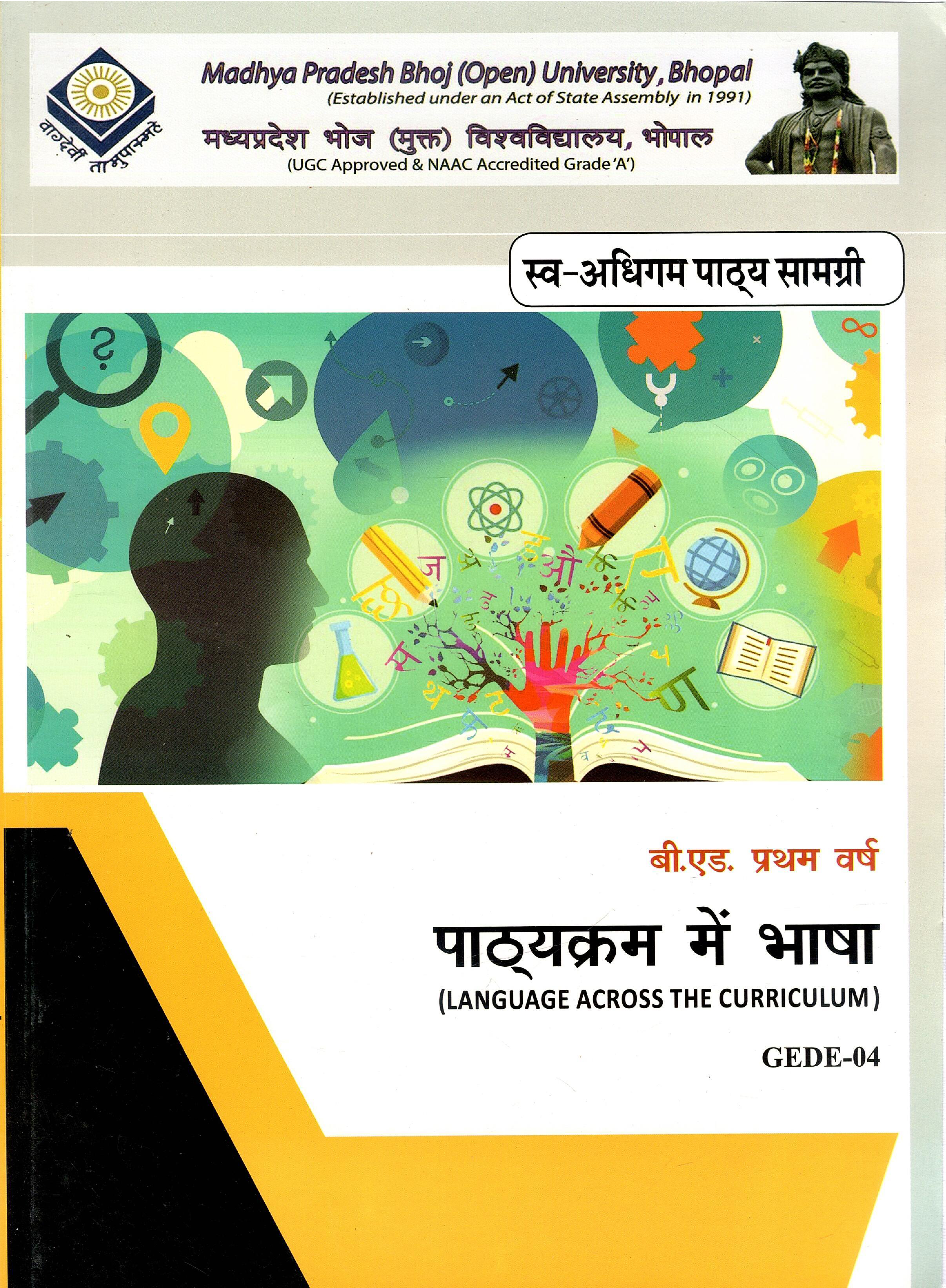Languages
भारतवाणी
bharatavani
bharatavani

Knowledge through Indian Languages












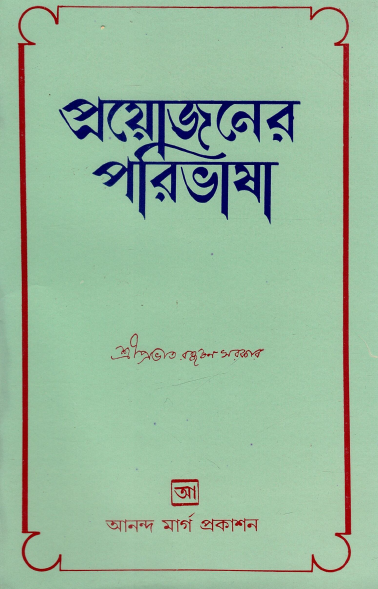

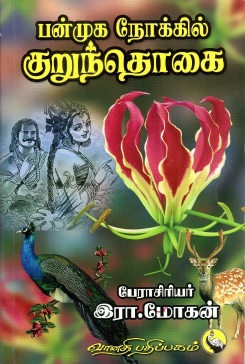


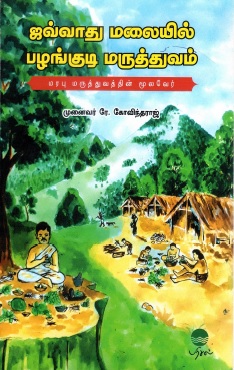

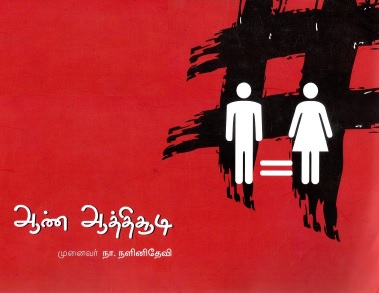
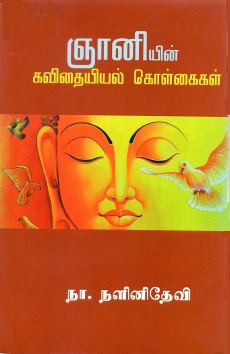

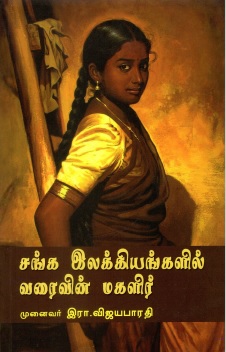

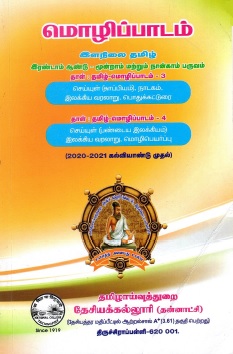
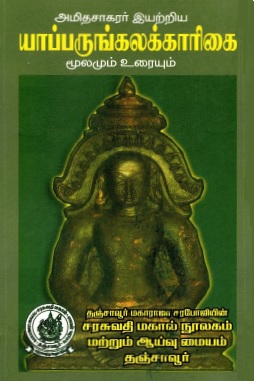
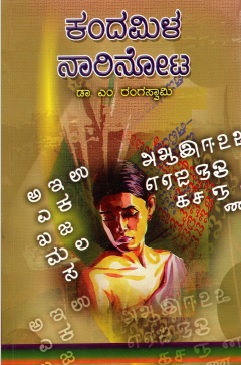
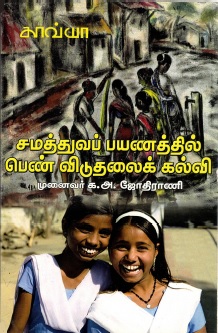
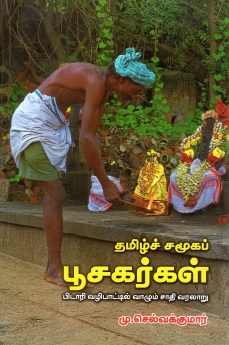
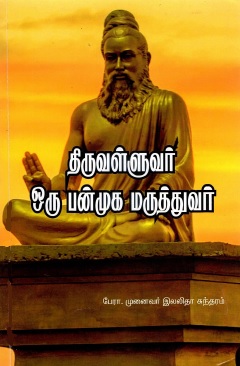
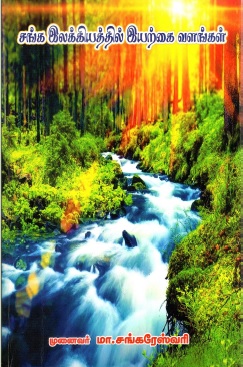
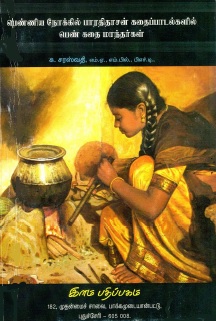
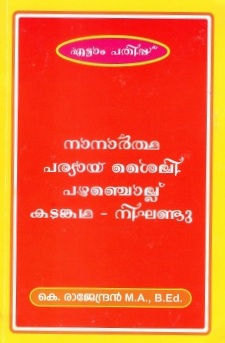
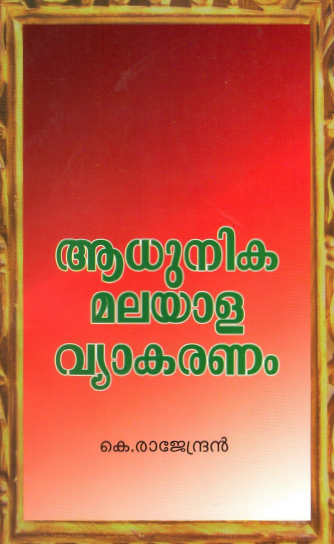
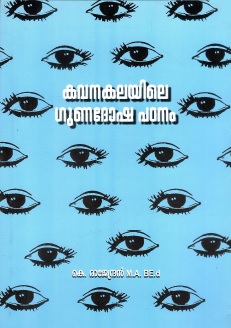

.jpg)
.jpg)
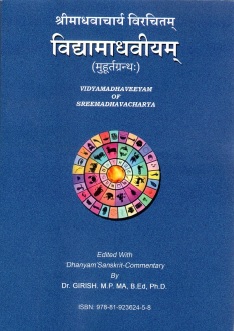
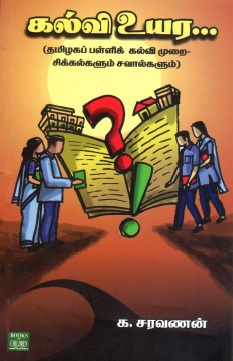
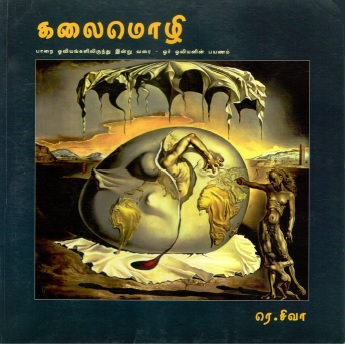
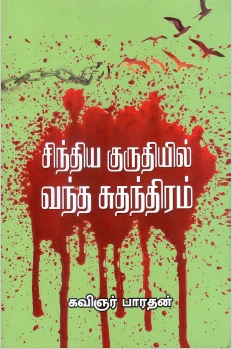
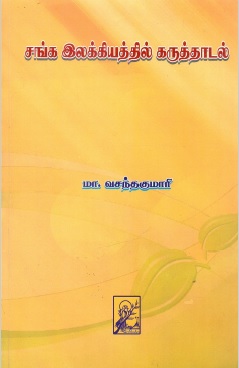
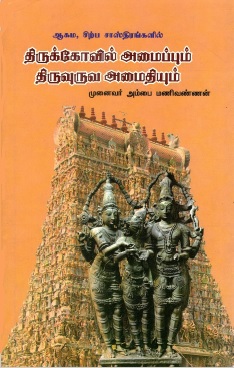

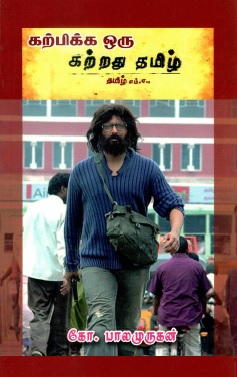
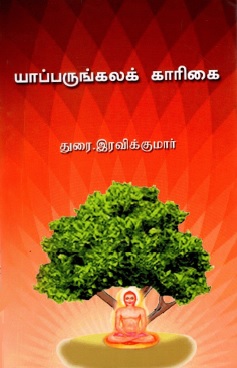
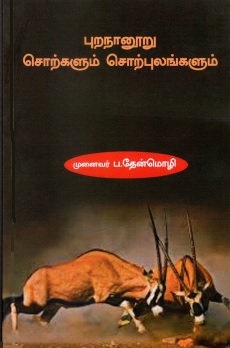
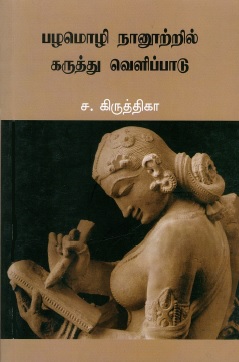
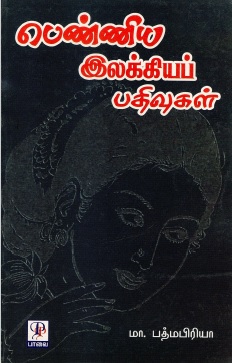

.jpg)

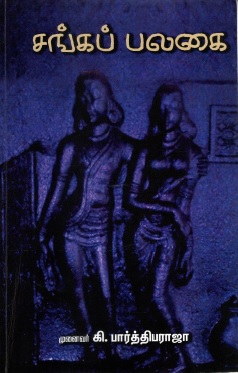
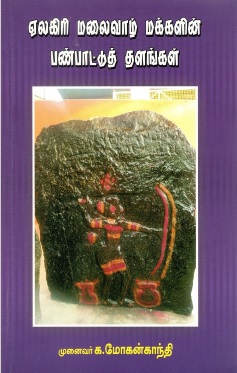
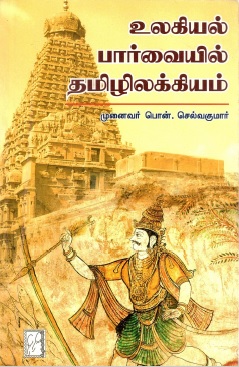
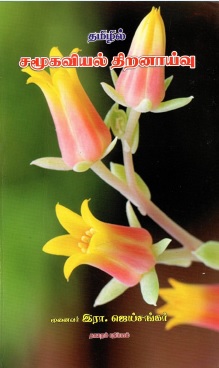
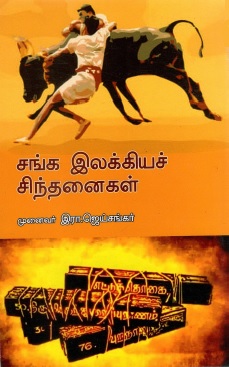

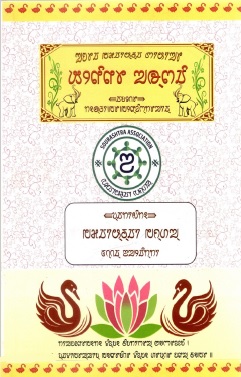

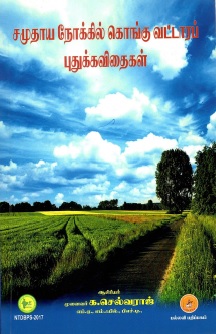
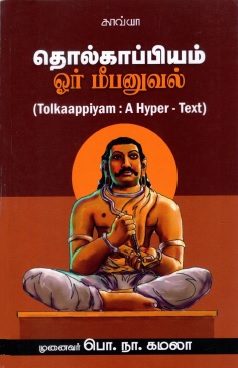

.jpg)
.jpg)
.jpg)
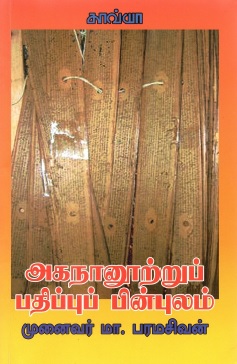
.jpg)
.jpg)