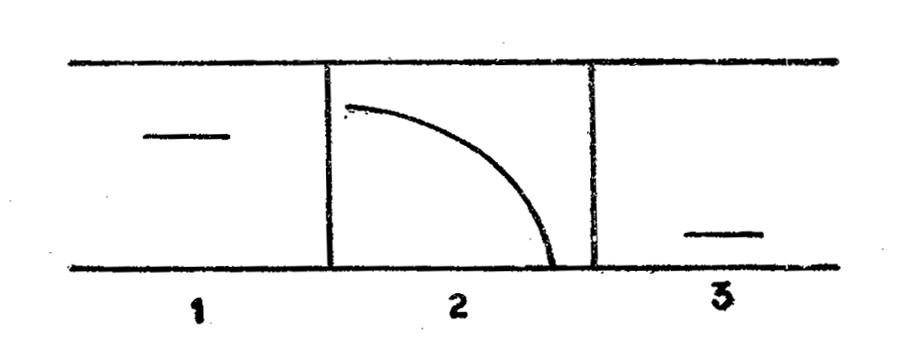भाषाएँ (हिंदी )
भारतवाणी
bharatavani
bharatavani

भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान